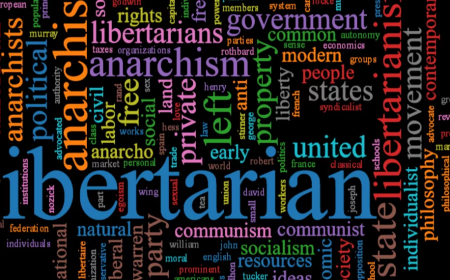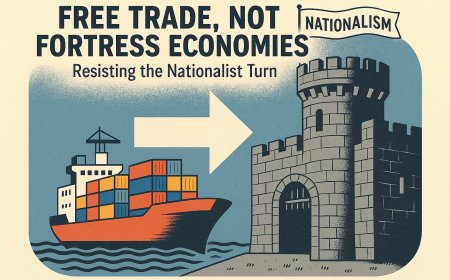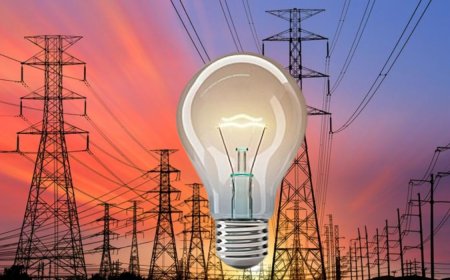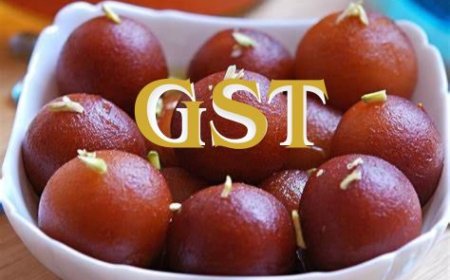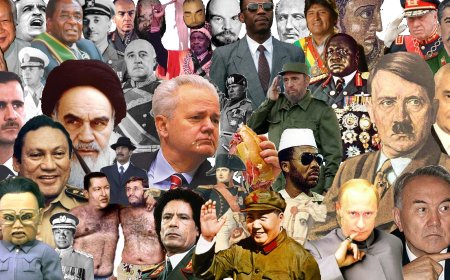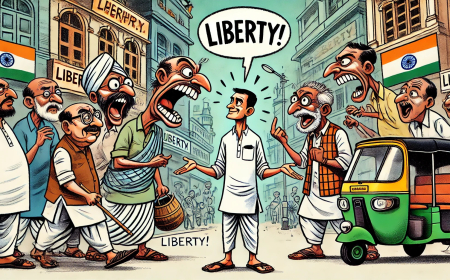मुक्त बाज़ार और मूल्य।
किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अंततः होता क्या है? क्या होता है जब राज्य किसी वस्तु का मूल्य तय करे?
अगर राज्य सर्वशक्तिशाली है तो क्या अपने बल प्रयोग से सभी को धनवान बना सकती है? क्या संसद में कानून बनाकर हमें न्यूटन के पहले नियम को निरस्त करना चाहिए? अगर यह प्रश्न आपको हास्यास्पद लग रहे है तो आपको अपने आस पास देखिए। राज्य इस प्रकार के प्रयोग प्रतिदिन कर रहा है और हमें उसके परिणाम झेलने पड़ रहे है।
राज्य(State) हमारे आधुनिक राजनीतिक तंत्र में एकमात्र संस्था है जो बल प्रयोग कर सकती है। इसे राजनैतिक शास्त्र में “हिंसा का एकाधिकार” कहते है। जैसे अग्नि और उसकी ताप को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राज्य और "हिंसा" या "बल प्रयोग"(coercion) को अलग नहीं किया जा सकता। नैतिक स्तर पर, राज्य के बल प्रयोग से मूल्य (दाम) की सीमा लागू करना गलत है क्योंकि यह दो वयस्कों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो अपनी सहमति से लेन-देन करना चाहते हैं। हालांकि नैतिकता ही राज्य द्वारा किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर हस्तक्षेप का अकेला गलत कारण नहीं है।
जब राज्य किसी वस्तु या सेवा के मूल्य की सीमा लागू करता है, तो यह आमतौर पर उत्पादन को हतोत्साहित करता है और मांग को बढ़ा देता है, क्योंकि जिस दाम पर सीमा लगी है उसपर बहुत लोग खरीदने तो तैयार है पर कोई उत्पादन करने तैयार नहीं होगा, जिससे उस वस्तु या सेवा की कमी हो जाती है। इसके अलावा, एक काला बाजार उभर आता है।
उदाहरण के लिए यदि कल सुबह मोदी जी उठकर कहे कि आज से अनार की कीमत 100 के बजाय 90 रूपये प्रति किलो है, क्योंकि यह गरीबों का अधिकार है कि वे अनार खा सके। उसी सुबह क्योंकि दाम पिछली सुबह से 10 रुपए कम हो गया है, अनारों की मांग बढ़ जाएगी। किन्तु इसी मूल्य पर या तो आपूर्ति(सप्लाई) घट जाएगा क्योंकि अब इस मूल्य पर विक्रेता का लाभ नहीं है, या उतनी ही रहेगी। इससे जल्द ही अनारों की कमी हो जाएगी। इस उदाहरण में राज्य ने बल प्रयोग कर विक्रेताओं को अनार 90 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर मजबूर किया।
इसके विपरीत, जब राज्य मूल्य न्यूनतम (फ्लोर) लागू करता है, तो उत्पादन बढ़ जाता है और मांग घट जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में इन्वेंटरी बच जाती है जिसे राज्य को खरीदना पड़ता है। मूल्य सीमा लागू करने पर, राजनैतिक दबाव यह सुनिश्चित करती है कि सभी को वस्तु तक पहुंच मिले, जिससे मूल्य का अर्थ खत्म हो जाता है। यह मूलतः पहले आओ, पहले पाओ की स्थिति बन जाती है।
मूल्य केवल खोजा जा सकता है। इसे "निर्धारित" नहीं किया जा सकता। यदि राज्य मूल्य "निर्धारित" करता है, तो वह मूल्य नहीं रह जाता। वह कुछ और बन जाता है। मूल्य का संबंध मूल्यांकन से है। मूल्यांकन सापेक्ष(subjective) होता है। जब कोई बेचता है और कोई खरीदता है, तो लेन-देन में दो सहमत वयस्क होते हैं, जहां खरीदार वस्तु को उस मूल्य से अधिक महत्व देता है जो वह चुका रहा है, और उत्पादक पैसे को उस वस्तु से अधिक महत्व देता है जो वह बेच रहा है। लेकिन वही वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी कारण से अधिक मूल्यवान हो सकती है, और वह अधिक मूल्य चुकाने को तैयार हो सकता है। इस प्रकार एक मुक्त बाजार में मूल्य प्राथमिकताओं को सुलझाते हैं और संसाधनों को वहां आवंटित करते हैं जहां आवश्यकता अधिक होती है।
लेकिन जब उड़ान टिकट की कीमत पर एक सीमा लगा दी जाती है, तो जो व्यक्ति सामान्यतः अपने घर जा रहा है, वह उसी टिकट के लिए उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करेगा जो अपने अस्पताल में भर्ती पिता के पास जाना चाहता है। मूल्य सीमा के कारण बाजार प्राथमिकताओं का मूल्यांकन नहीं कर सकता, जिससे अस्पताल में भर्ती पिता के बेटे के लिए टिकट की कमी हो जाती है।
मुक्त बाजार में प्राथमिकताओं का मूल्यांकन होता है। मूल्य का एक और महत्व यह है कि जब यह बढ़ता है, तो यह दूसरों को बाजार में आने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मांग पूरी होती है और कीमत कम हो जाती है। किसी आपदा या आपातकाल में जब कीमतें बढ़ती हैं, तो यह अच्छा होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्ति आएगी। जब एक प्लंबर देखता है कि सफाईकर्मियों के वेतन बढ़ रही हैं, तो वह अपने स्वार्थ में वहां काम करता है, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाती है।
मूल्य एक निर्णय लेने का उपकरण है। यह सभी उपलब्ध सूचनाओं का संग्रह है जो उन्हें स्वार्थ में तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। मूल्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद का माध्यम है, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। रेंट कंट्रोल, एमआरपी, एमएसपी, न्यूनतम वेतन – ये सभी अनैतिक और विनाशकारी हैं। भारत में न्यूनतम वेतन लगभग ₹13,000 प्रति माह है। इसके प्रभाव वही हैं जो मूल्य न्यूनतम लागू करने पर होते हैं – अधिक आपूर्ति और बहुत कम मांग। श्रम के मामले में इसका मतलब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, खासकर औपचारिक क्षेत्र में। इससे कम वेतन वाले स्थानों पर अकुशल कार्य का आउटसोर्सिंग होता है। दूसरा, चूंकि मनरेगा न्यूनतम वेतन देती है, यह एक अपेक्षा निर्धारित करती है, जिससे कम वेतन पर कोई काम नहीं करना चाहता और अकुशल मजदूरों को काम पर रखना अव्यवहारिक हो जाता है।
मूल्य का उतार-चढ़ाव संसाधन आवंटन(रिसोर्स एलोकेशन) को नए सिरे से व्यवस्थित करने की ध्वनि है।
What's Your Reaction?